जानिए हमारा कानून
क्या CrPC की धारा 207 के तहत अभियुक्त को संरक्षित गवाहों के संशोधित बयान की प्रति दी जा सकती है?
हमारे न्याय तंत्र में यह एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त (Accused) को निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का अधिकार कैसे दिया जाए। आतंकवाद और संगठित अपराध (Organized Crime) जैसे मामलों में यह मुद्दा और जटिल हो जाता है, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।Waheed-ur-Rehman Parra v. Union Territory of Jammu & Kashmir (2022) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन जटिलताओं पर प्रकाश डाला और दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure - CrPC),...
धारा 40-A, राजस्थान आबकारी अधिनियम: राजस्व की विशेष वसूली का प्रावधान
राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 40-A में राज्य सरकार को आबकारी राजस्व (Excise Revenue) की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। यह प्रावधान उन मामलों में लागू होता है, जहां डिफॉल्टर (Defaulter) समय पर राजस्व का भुगतान नहीं करता।इस धारा के तहत, जिला आबकारी अधिकारी (District Excise Officer) को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों से वसूली कर सकें, जो डिफॉल्टर को पैसे देने वाले हों। यह लेख धारा 40-A की हर बारीकी को सरल हिंदी में समझाता है। डिफॉल्टर का अर्थ (Meaning of...
मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 340 और 341
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को मान्यता देती है।धारा 340 और 341 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती हैं कि किसी आरोपी को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है और अगर वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो राज्य द्वारा उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान न्याय तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। धारा 340: अपनी पसंद के वकील का अधिकार (Right to Choose an Advocate) धारा 340 यह मान्यता देती है...
आर्म्स एक्ट की धारा 45: कब यह कानून लागू नहीं होता?
आर्म्स एक्ट, 1959 भारत में हथियारों और गोला-बारूद (arms and ammunition) के स्वामित्व, निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करता है। यह कानून जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों और व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता। इन अपवादों (exemptions) को धारा 45 में विस्तार से बताया गया है। यह लेख इन अपवादों को सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करता है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। धारा 45 का उद्देश्य और दायरा (Scope of...
झूठे निशान लगाने के अपराध: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 350
झूठे निशानों (False Marks) से जुड़े अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) की धारा 350 विशेष ध्यान देती है। यह प्रावधान धोखाधड़ी, व्यापारिक ईमानदारी और उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।धारा 350 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of Section 350) धारा 350(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु (Goods) के मामले, पैकेज (Package) या कंटेनर (Receptacle) पर ऐसा झूठा निशान लगाता है जो किसी सार्वजनिक सेवक (Public Servant) या अन्य व्यक्ति को यह...
Transfer Of Property Act में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का हक़ नहीं रखने की Condition होने पर ट्रांसफर के बाद में हक़ उत्पन्न होना
इस एक्ट की धारा 43 के प्रावधानों में यह भी शामिल है कि अन्तरक अन्तरण के पश्चात् अन्तरित सम्पत्ति में हित अर्जित कर सकता है। यह सम्पत्ति ही अनुपोषण की विषयवस्तु होगी। अन्तरक द्वारा बाद में अर्जित कोई अन्य सम्पति जो न तो अन्तरण की विषयवस्तु थी और न ही जिसे अन्तरित करने को प्रव्यंजना अन्तरक ने की थी अनुपोषण की विषयवस्तु नहीं होगी, भले ही इसकी प्राप्ति मिथ्याव्यपदेशन जाहिर होने के बाद हुई हो। इसी प्रकार यदि अन्तरक ने एक हैसियत से सम्पत्ति अन्तरित की थी तथा दूसरी हैसियत से सम्पत्ति अर्जित करता है...
Transfer Of Property Act में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होकर भी संपत्ति ट्रांसफर की जानी
इस एक्ट की धारा 43 Unauthorized Person द्वारा अंतरण के विषय में उल्लेख कर रही है। इस धारा का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का अंतरण उस समय कर देता है जिस समय वह इस प्रकार का अंतरण करने के लिए अधिकृत नहीं है परंतु बाद में वह संपत्ति का अंतरण करने के लिए अधिकृत हो जाता है तब इस अधिनियम के क्या प्रावधान होंगे वे सभी प्रावधान इस धारा में समाहित किए गए हैं।यदि अन्तरण विलेख में, जिसे पक्षकारों के बीच तैयार किया गया है और जिसे उनकी मुहर द्वारा सत्यापित किया गया है किसी तथ्य का उल्लेख है और...
आपराधिक मामलों में लोक अभियोजक की भूमिका और अभियोजन का संचालन करने की अनुमति : धारा 338 और 339 BNSS, 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।इसमें धारा 338 और 339 अभियोजन (Prosecution) के संचालन और उससे जुड़े पक्षों की भूमिकाओं को स्पष्ट करती हैं। ये प्रावधान इस बात का ध्यान रखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में राज्य, पीड़ित और अन्य पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन बना रहे। धारा 338: लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) की भूमिका धारा 338(1) धारा 338 के...
हथियारों की जनगणना और शक्तियों के हस्तांतरण से जुड़े प्रावधान: आर्म्स एक्ट, 1959 की धाराएं 42 और 43
आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) भारत में हथियारों और गोला-बारूद के नियमन के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून की धाराएं 42 और 43 सरकार को हथियारों की जनगणना (Census) करने और शक्तियों को अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपने का अधिकार देती हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।धारा 42: हथियारों की जनगणना करने की शक्ति (Power to Take Census of Firearms)धारा 42 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष क्षेत्र में...
राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 40: आबकारी राजस्व की वसूली की प्रक्रिया और डिफॉल्टर की जिम्मेदारी
आबकारी राजस्व (Excise Revenue) की वसूली राजस्थान आबकारी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह राज्य सरकार को आबकारी से संबंधित बकाया राशि को कुशलतापूर्वक एकत्रित करने का अधिकार देता है।अधिनियम की धारा 40 (Section 40) इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाती है। इस लेख में, धारा 40 के प्रावधानों को सरल हिंदी में समझाया गया है ताकि इसे आम लोग भी आसानी से समझ सकें। आबकारी राजस्व (Excise Revenue) क्या है?आबकारी राजस्व वह आय है, जो राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के माध्यम से प्राप्त होती है।...
नकली संपत्ति चिह्न वाले सामान की बिक्री: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 349
धारा 349 का उद्देश्य और इसके प्रावधानभारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के तहत धारा 349 नकली संपत्ति चिह्न (Counterfeit Property Mark) लगे सामान की बिक्री, उसे बेचने के लिए प्रदर्शित करने या भंडारण करने को अपराध घोषित करती है। यह प्रावधान उपभोक्ताओं की सुरक्षा, बाजार की विश्वसनीयता और व्यापार में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। धारा 349 के तहत अपराध के तत्व धारा 349 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है: 1. किसी सामान या वस्तु...
Transfer Of Property Act में बेनामी संपत्ति का उदाहरण
वास्तविक स्वामी की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से Ostensible Owner हो इस सिद्धान्त का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि अन्तरक वास्तविक स्वामी की स्पष्ट या विवक्षित सम्मति से Ostensible Owner हो सम्मति देते समय यह आवश्यक है कि वास्तविक स्वामी बालिग, शुद्धचित्त एवं सामान्य प्रकृति का हो नाबालिग उन्मत्त या विकृत चित्त वाले व्यक्तियों की सम्मति इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त नहीं होगी। इसी प्रकार वास्तविक स्वामी की मूक सम्मति (Acquiscence) भी इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त नहीं है। उसका दायित्व इस बात पर निर्भर करता...
Transfer Of Property Act में प्रॉपर्टी का बेनामी मालिक किसे माना जाता है?
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 Ostensible Owner के संबंध में प्रावधान उपलब्ध करती है। जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है दृश्यमान का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का असल स्वामी नहीं है परंतु वे संपत्ति का स्वामी प्रतीत होता है। साधारण भाषा पर इसे संपत्ति का नकली स्वामी कहा जा सकता है। इसके संबंध में भारत में बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 भी निर्माण किया गया है। Ostensible Owner ऐसा स्वामी है जो स्वामी तो दिखाई पड़ रहा है परंतु संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है अनेकों प्रकरण में...
धारा 10, 11 ,13, 14 और 15 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022, भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों (Unfair Means) को रोकने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। यह कानून कड़ी सज़ा, जवाबदेही, और जाँच की प्रक्रिया पर जोर देता है, ताकि परीक्षा की गरिमा और विश्वास बहाल किया जा सके।अनुचित साधनों पर सज़ा (Penalties for Unfair Means) धारा 10(1) के तहत, जो परीक्षार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं, उन्हें तीन साल तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया...
सेक्शन 12, 16 और 17 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित तरीकों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।इसमें संपत्ति कुर्की (Attachment) और जब्ती (Confiscation) के प्रावधानों के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया के लिए नामित न्यायालयों (Designated Courts) की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस लेख में अधिनियम के सेक्शन 12, 16 और 17 का सरल हिंदी में विवरण दिया गया है। सेक्शन 12: संपत्ति की कुर्की और जब्ती संपत्ति कुर्की और जब्ती का उद्देश्य सेक्शन...
जब्ती के लिए जिम्मेदार वस्तुएं: राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 69
राजस्थान एक्साइज़ अधिनियम (Rajasthan Excise Act) की धारा 69 में उन वस्तुओं, साधनों और संपत्तियों का वर्णन किया गया है जो अधिनियम के तहत अपराध होने पर जब्त (Confiscation) की जा सकती हैं।इस लेख में, हम इस धारा को सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आम पाठक इसे आसानी से समझ सकें। कठिन हिंदी शब्दों के लिए उनके अंग्रेजी समकक्ष (Equivalent) का भी उल्लेख किया गया है। 1. धारा 69(1): अपराध के लिए जिम्मेदार वस्तुएं (Liable Articles) इस धारा के अनुसार, जब भी राजस्थान एक्साइज़ अधिनियम के तहत कोई...
धारा 70 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों का समाधान और जब्त संपत्ति
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (Rajasthan Excise Act) के तहत आबकारी अधिकारियों (Excise Officers) को कुछ अपराधों का निपटारा (Resolution) करने की शक्ति दी गई है। धारा 70 के तहत, ऐसे अपराधों का समाधान पैसे के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को छोटा और सरल बनाया जा सके। इस लेख में इस प्रावधान को सरल हिंदी में समझाया गया है।अपराधों का समाधान करने की शक्ति (Power to Compound Offences) धारा 70(1) के अनुसार, आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य...
Know The Law | अनधिकृत लेनदेन के कारण ग्राहकों के पैसे खोने पर बैंकों की जिम्मेदारी
ग्राहक के बैंक खाते में दर्ज धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की जिम्मेदारी बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों से दर्ज अनधिकृत लेनदेन से बचाने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।यह आदेश एक ऐसे ग्राहक के मामले में पारित किया गया, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग की और बाद में आइटम वापस करने की कोशिश की। उसने रिटेलर के कस्टमर केयर के रूप में खुद को पेश करने वाले धोखेबाज से कॉल के बाद एक ऐप डाउनलोड किया, जिसके कारण कुल 94,204.80 रुपये का...
Transfer Of Property Act की धारा 40 के प्रावधान
Transfer Of Property Act की धारा 40 के अनुसार-'ख' को सुल्तानपुर बेचने की संविदा 'क' करता है। संविदा के प्रवर्तन में होते हुए भी वह सुल्तानपुर 'ग' को जिसे संविदा को सूचना है, बेच देता है। 'ख' संविदा को 'ग' के विरुद्ध उसी विस्तार तक प्रवर्तित करा सकेगा जिस तक वह 'क' के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है।इस धारा में हेउड बनाम अंसविक बिल्डिंग सोसाइटी नामक वाद में प्रतिपादित सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है। इसके अन्तर्गत स्वीकारात्मक संविदाओं को अन्तरक से सम्पत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध...
Transfer Of Property Act में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के उदाहरण
डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे अ अपनी तीन सम्पत्तियों x y तथा z 'ब' को एक ही संव्यवहार द्वारा अन्तरित करता है तथा 'ब' की सम्पत्ति P. स को देता है। अन्तरण विलेख में यह उल्लिखित है कि सम्पत्ति x सम्पत्ति P के एवज में दी जा रही है। यदि व सम्पत्ति P को हो धारण किये रहना स्वीकारता है तो वह केवल सम्पत्ति नहीं पायेगा। शेष दोनों सम्पत्तियों y तथा z को अपनी विसम्मति व्यक्त करने के बावजूद भी पाने का अधिकारी होगा।वैवाहिक समझौते के तहत, यदि अ की पत्नी उसकी मृत्यु के समय...



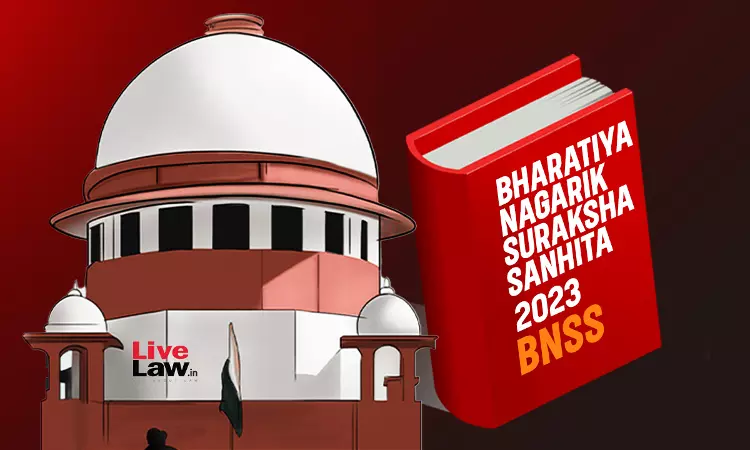




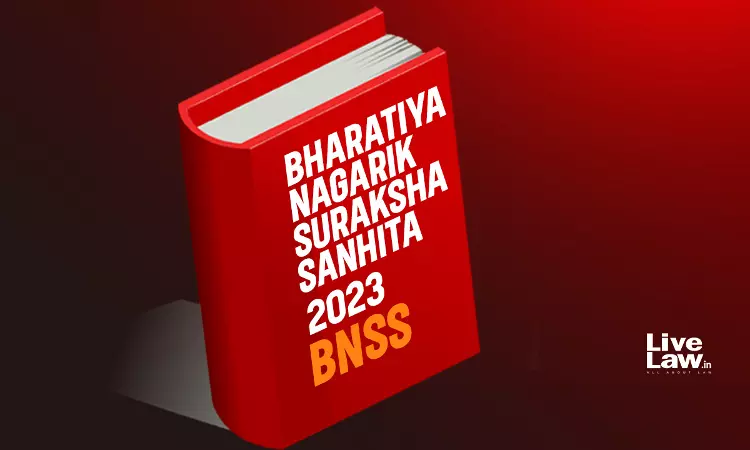

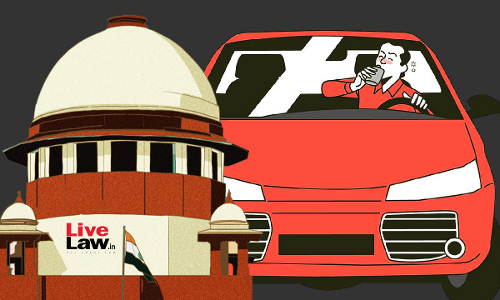
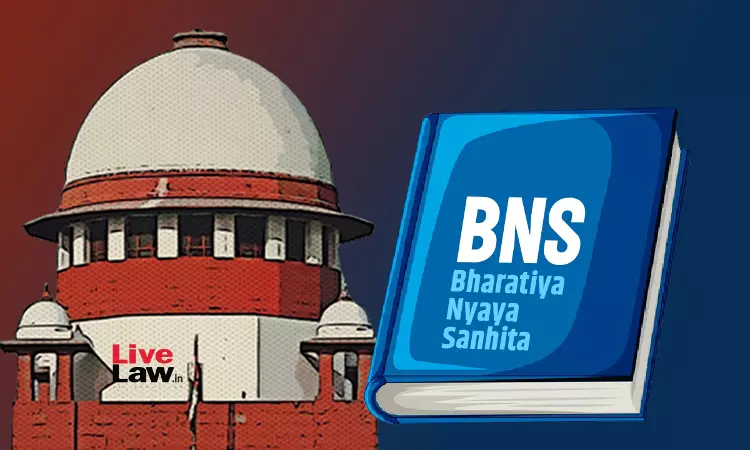

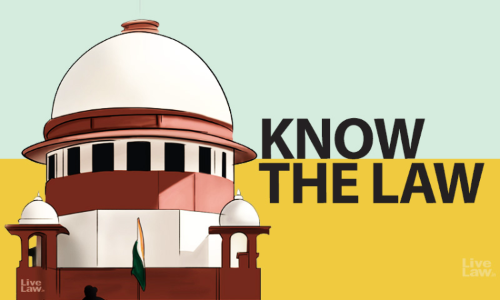

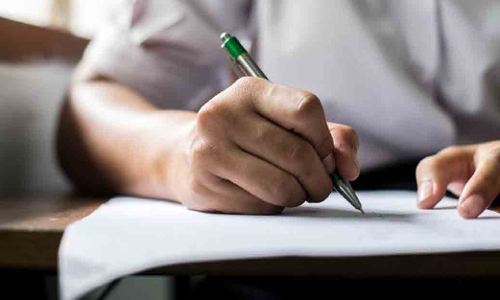


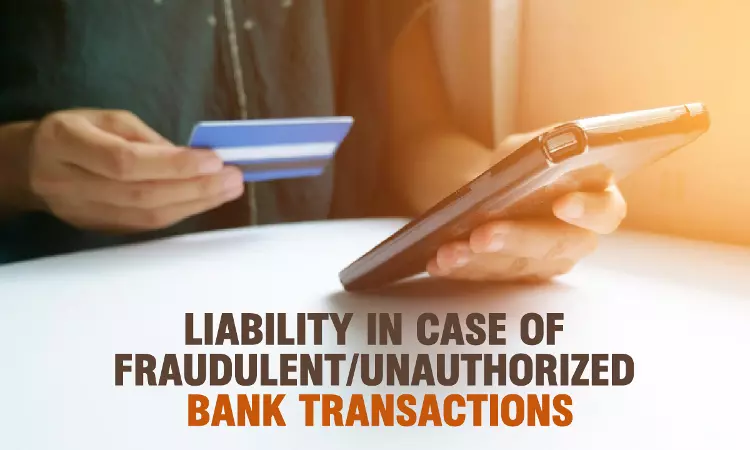




 Advertise with us
Advertise with us