भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 457: कारावास से संबंधित प्रावधान
Himanshu Mishra
12 May 2025 1:20 PM IST
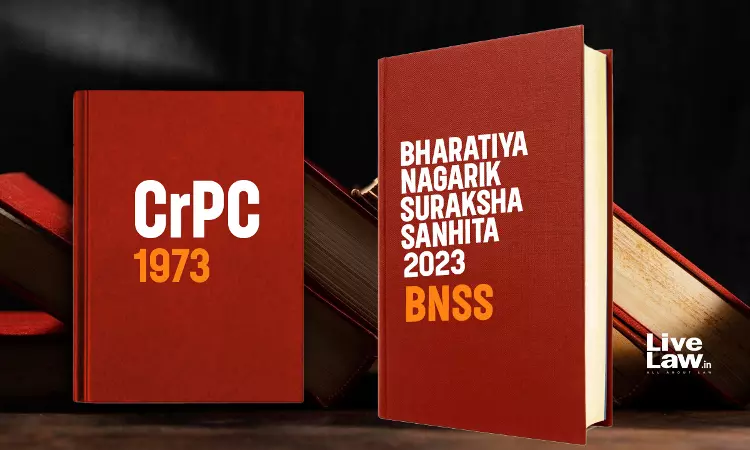
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के अध्याय XXXIV (धारा 453 से 462) में दंडों के निष्पादन (Execution), स्थगन (Suspension), क्षमादान (Remission), और रूपांतरण (Commutation) से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं।
इसी क्रम में धारा 457 'कारावास' (Imprisonment) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। यह धारा बताती है कि किस स्थान पर किसी दोषी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा जाएगा, और नागरिक कारागार (Civil Jail) से आपराधिक कारागार (Criminal Jail) में स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होगी।
इस लेख में हम धारा 457 के प्रत्येक उपखंड को विस्तार से समझेंगे, उसका व्यावहारिक महत्व बताएंगे और जहां आवश्यक होगा, वहां उदाहरणों (Illustrations) की मदद से भी स्पष्टीकरण देंगे। साथ ही, संहिता की पूर्ववर्ती धाराओं से इसका संबंध भी स्पष्ट करेंगे।
धारा 457(1) – कारावास के स्थान का निर्धारण करने की राज्य सरकार की शक्ति
धारा 457 की उपधारा (1) के अनुसार, जब तक किसी अन्य कानून में कुछ भिन्न रूप से न कहा गया हो, तब तक राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह यह निर्देश दे सके कि इस संहिता के अंतर्गत कारावास योग्य किसी व्यक्ति को किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा जाएगा।
इसका अर्थ यह है कि किसी दोषी व्यक्ति को कहां बंदी बनाकर रखा जाए – जैसे जिला कारागार, केंद्रीय कारागार, विशेष सुरक्षा कारागार आदि – इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार के पास होता है। हालांकि, यदि किसी विशेष कानून में कोई अलग प्रावधान हो, तो उस विशेष कानून का पालन किया जाएगा।
उदाहरण
मान लीजिए कि एक व्यक्ति को धारा 409 (मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में भेजे जाने वाले मामले) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अब राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि उस व्यक्ति को जयपुर केंद्रीय कारागार में रखा जाएगा या किसी अन्य उपयुक्त जेल में।
धारा 457(2) – सिविल जेल में बंद व्यक्ति को आपराधिक जेल में स्थानांतरित करना
इस उपधारा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के अंतर्गत कारावास योग्य है या हिरासत में लिया गया है और वह वर्तमान में किसी सिविल जेल में बंद है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट जिसे उसे कारावास या हिरासत में भेजने का आदेश देने का अधिकार है, वह यह निर्देश दे सकता है कि उस व्यक्ति को आपराधिक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति जो अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह सामान्य दीवानी (Civil) कैदियों के साथ नहीं रखा जाए, क्योंकि आपराधिक दोषियों के लिए अलग जेल प्रणाली होती है। इससे जेल प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
उदाहरण
मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिविल प्रकृति के मामले में बंदी बनाया गया था, लेकिन उसी व्यक्ति के विरुद्ध अब आपराधिक संहिता के अंतर्गत गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध हो गया और उसे जेल भेजने का आदेश हुआ। ऐसे में मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि उसे आपराधिक जेल में भेजा जाए।
धारा 457(3) – आपराधिक जेल से सिविल जेल में वापसी
धारा 457 की तीसरी उपधारा बताती है कि जब किसी व्यक्ति को उपधारा (2) के अंतर्गत आपराधिक जेल में भेज दिया जाता है, तो उसकी रिहाई के बाद उसे दोबारा सिविल जेल में भेजा जाएगा।
हालांकि, इसके दो अपवाद (Exception) हैं—
पहला अपवाद – तीन वर्षों की अवधि बीत जाना:
यदि व्यक्ति को आपराधिक जेल में भेजे जाने के बाद तीन वर्ष बीत चुके हैं, तो उसे यह मान लिया जाएगा कि वह सिविल जेल से भी मुक्त हो चुका है। यह व्यवस्था दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 58 के तहत की गई है।
दूसरा अपवाद – अदालत द्वारा प्रमाण पत्र देना:
यदि उस व्यक्ति को सिविल जेल भेजने वाली अदालत आपराधिक जेल के प्रभारी अधिकारी को प्रमाण पत्र दे देती है कि वह व्यक्ति अब दीवानी प्रकृति की सजा से मुक्त होने का अधिकारी है, तो उसे सिविल जेल में वापस नहीं भेजा जाएगा।
उदाहरण
एक व्यापारी को दीवानी मुकदमे में भुगतान न करने के कारण सिविल जेल में बंद किया गया था। बाद में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का एक आपराधिक मामला सिद्ध हुआ और उसे आपराधिक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यदि तीन साल तक वह आपराधिक जेल में रहा, तो उसे दीवानी जेल से भी मुक्त माना जाएगा और उसे फिर से सिविल जेल में नहीं भेजा जाएगा।
सम्बन्धित पूर्ववर्ती धाराओं का संदर्भ
धारा 453 से 456 में जहां मृत्युदंड (Death Sentence) की पुष्टि, निष्पादन, और स्थगन की प्रक्रिया बताई गई है, वहीं धारा 457 से कारावास की प्रकृति और स्थान पर प्रकाश डाला गया है। संपूर्ण अध्याय XXXIV न्यायिक आदेशों के अमल को सुनिश्चित करने और दोषियों की सजा को उचित स्थान पर लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
उदाहरण के लिए, धारा 453 में स्पष्ट किया गया है कि जब उच्च न्यायालय किसी मृत्युदंड को पुष्टि करता है, तो सत्र न्यायालय (Court of Session) को उस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों में भी दोषी को विशेष सुरक्षा वाले कारागार में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसका निर्देश धारा 457 के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।
व्यावहारिक दृष्टिकोण से धारा 457 का महत्व
धारा 457 एक प्रशासनिक धारा है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रभाव है। यह जेल प्रशासन को नियंत्रित करती है, बंदियों की उपयुक्त श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण सुनिश्चित करती है, और सजा के निष्पादन में व्यवस्था बनाए रखती है।
यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि दोषियों के पुनर्वास, सुधार और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें उपयुक्त जेल में रखा जाए। साथ ही, यह दीवानी और आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच समन्वय को भी बनाए रखती है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 457 जेलों की व्यवस्था और दोषियों की श्रेणी के अनुसार उनकी बंदी व्यवस्था से संबंधित एक व्यापक और संतुलित प्रावधान है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और जेल प्रशासन तीनों के बीच आवश्यक सामंजस्य स्थापित करती है। दीवानी और आपराधिक मुकदमों में बंद किए गए व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान पर रखने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है, जिससे न केवल न्याय की निष्पक्षता बनी रहती है बल्कि सुधारात्मक न्याय प्रणाली को भी बल मिलता है।





 Advertise with us
Advertise with us