धारा 431 BNSS 2023: दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी
Himanshu Mishra
23 April 2025 6:41 PM IST
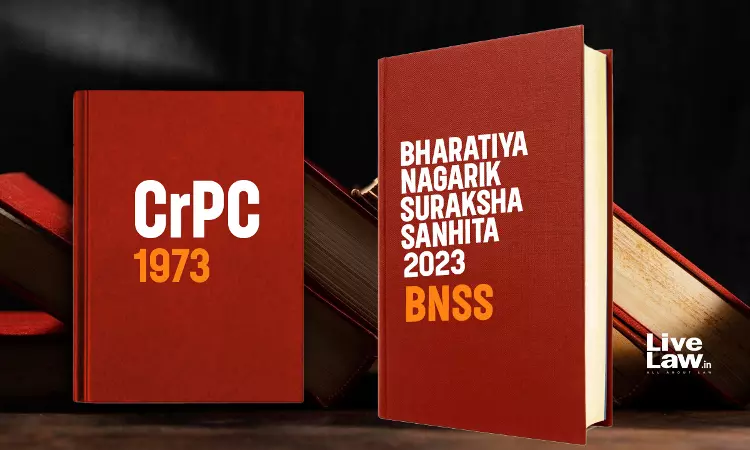
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए।
लेकिन जब कोई अभियुक्त निचली अदालत (Lower Court) से दोषमुक्त (Acquitted) हो जाता है, और अभियोजन पक्ष (Prosecution) या राज्य सरकार (State Government) उसके विरुद्ध हाईकोर्ट (High Court) में अपील (Appeal) करती है, तब यह प्रश्न उठता है कि उस दोषमुक्त व्यक्ति को क्या दोबारा न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है? इसी स्थिति के लिए भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 431 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
धारा 431 की पृष्ठभूमि और उद्देश्य (Background and Object of Section 431)
धारा 431 विशेष रूप से धारा 419 (Section 419) से संबंधित है, जो अभियुक्त के दोषमुक्त किए जाने पर उसके विरुद्ध अपील (Appeal against acquittal) को सक्षम बनाती है। जब हाईकोर्ट यह मानता है कि निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करना गलत था, तो वह उसके खिलाफ अपील को सुनने के लिए उसे न्यायालय में उपस्थित कराना आवश्यक समझ सकता है। इस उद्देश्य से, हाईकोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह एक गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी कर सके।
गिरफ्तारी का आदेश (Issuance of Warrant)
जब भी धारा 419 के अंतर्गत दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील हाईकोर्ट में की जाती है, तो हाईकोर्ट यह अधिकार रखता है कि वह एक वारंट (Warrant) जारी करे। इस वारंट के माध्यम से वह आदेश दे सकता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
यह अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि अभियुक्त को स्वतः समन या नोटिस भेजने पर वह उपस्थित नहीं होता, तो अपील की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। गिरफ्तारी के आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपील की सुनवाई प्रभावी रूप से हो सके और अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से बच न सके।
किस न्यायालय में लाया जा सकता है अभियुक्त को? (To Which Court Can the Accused Be Brought?)
धारा 431 के अंतर्गत हाईकोर्ट अभियुक्त को दो विकल्पों में से किसी एक के समक्ष प्रस्तुत कराने का आदेश दे सकता है:
1. हाईकोर्ट स्वयं (The High Court itself)
2. कोई अधीनस्थ न्यायालय (Any Subordinate Court)
यदि अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह न्यायालय यह अधिकार रखता है कि वह अभियुक्त को हिरासत (Custody) में भेज दे या फिर उसे जमानत (Bail) पर छोड़ दे।
हिरासत या जमानत – न्यायालय का विवेक (Custody or Bail – Discretion of Court)
अधीनस्थ न्यायालय या हाईकोर्ट, अभियुक्त को हिरासत में रखने या जमानत पर रिहा करने का निर्णय अपने विवेक (Discretion) से ले सकता है।
यह निर्णय कई बातों पर निर्भर करेगा जैसे कि:
• अभियुक्त का अपराध कितना गंभीर है?
• क्या अभियुक्त न्यायालय में पुनः उपस्थित होने की संभावना रखता है?
• क्या अभियुक्त के भागने की आशंका है?
• क्या वह पहले न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर चुका है?
यदि अभियुक्त गंभीर अपराध (Grave Offence) में दोषमुक्त हुआ है, तो उसे हिरासत में भेजा जाना अधिक संभावित होता है, लेकिन यदि मामला अपेक्षाकृत हल्का है, और अभियुक्त ने न्यायालय की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग किया है, तो उसे जमानत दी जा सकती है।
उदाहरण से समझिए (Understanding through Illustration)
मान लीजिए कि एक व्यक्ति 'अमित' पर हत्या (Murder) का आरोप था, लेकिन सत्र न्यायालय (Sessions Court) ने उसे साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार इस निर्णय से असंतुष्ट है और हाईकोर्ट में धारा 419 के तहत अपील दायर करती है। इस स्थिति में, हाईकोर्ट धारा 431 के तहत आदेश दे सकता है कि अमित को गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष लाया जाए। हाईकोर्ट यदि उपयुक्त समझे, तो वह अमित को जिला न्यायालय (Subordinate Court) के समक्ष भी भेज सकता है, जो उसे हिरासत में या जमानत पर रखने का निर्णय करेगा।
अन्य प्रासंगिक धाराएं (Related Sections)
इस विषय को बेहतर समझने के लिए धारा 419 को देखना आवश्यक है, जो कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, धारा 423 और 424 भी महत्वपूर्ण हैं, जो अपील दायर करने की प्रक्रिया (Filing of Appeal) और जेल में बंद अभियुक्तों के लिए अपील की व्यवस्था करती हैं।
धारा 425 में अपील की प्रारंभिक जांच (Summary Dismissal) का प्रावधान है, और धारा 426 अपील की नियमित सुनवाई (Regular Hearing) से संबंधित है। यदि इन प्रक्रियाओं के दौरान यह आवश्यक हो कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जाए, तो धारा 431 अत्यंत प्रासंगिक बन जाती है।
धारा 431 यह सुनिश्चित करती है कि जब भी किसी अभियुक्त के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की जाती है, तो वह अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) से बच न सके और न्यायालय की सुनवाई में उपस्थित हो सके। यह न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) और अभियुक्त के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।
यह धारा न केवल अपील की निष्पक्षता को बनाए रखने में सहायक है, बल्कि यह अभियुक्त को यह संदेश भी देती है कि दोषमुक्ति अंतिम निर्णय नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना, न्याय के प्रति उसका उत्तरदायित्व भी है।





 Advertise with us
Advertise with us