सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 177: आदेश 32 नियम 7 के प्रावधान
Shadab Salim
27 May 2024 10:00 AM IST
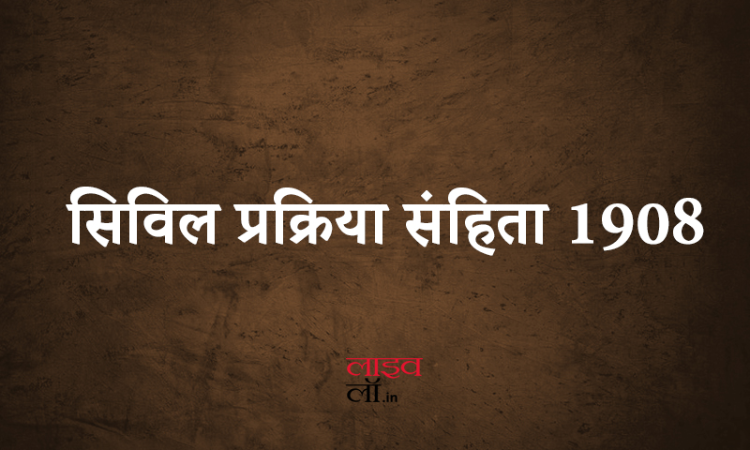
सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 7 पर प्रकाश डाला जा रहा है।
नियम-7 वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा करार या समझौता (1) कोई भी वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से कोई करार या समझौता उस वाद के बारे में जिसमें वाद-मित्र या संरक्षक की हैसियत में वह कार्य करता है, न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं करेगा जो इजाजत कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित की जाएगी।
(1क) उपनियम (1) के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ, यथास्थिति, वादमित्र या वादार्थ संरक्षक का शपथपत्र होगा और यदि अवयस्क का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किया जाता है तो, प्लीडर का इस आशय का प्रमाणपत्र भी होगा कि प्रस्थापित करार या समझौता उसकी राय में अवयस्क के फायदे के लिए किया गया है :
परन्तु शपथपत्र या प्रमाणपत्र में इस प्रकार अभिव्यक्त की गई राय, न्यायालय को यह जांच करने से प्रवारित नहीं करेगी कि क्या प्रस्थापित करार या समझौता अवयस्क के फायदे के लिए है।
(2) न्यायालय की इस प्रकार अभिलिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्यकरणीय होगा।
नियम 7 अवयस्क की ओर से उसके वादमित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा उस वाद में करार या समझौता करने की शर्तें निर्धारित करता है।
इस नियम में नया उपनियम (1क) तथा परन्तुक जोड़ा गया है, जो शपथपत्र व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भी न्यायालय द्वारा जांच के द्वार खोलता है।
नियम 7 का परिक्षेत्र व विस्तार- समझौता डिक्री एक अवयस्क पर कब बाध्यकारी
आदेश 32 के नियम 7 में जो शर्तें बताई गई हैं, उनमें न्यायालय की इजाजत लेना आवश्यक है, जो कि एक अवयस्क के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। न्यायालयों के पुराने मतभेदों को सुलझाने के लिए नियम 7 में 1976 में संशोधन कर उपनियम (1क) तथा उसके साथ एक परन्तुक जोड़ दिया गया है।
इस प्रकार नियम 7 में निम्नलिखित शर्ते दी गई हैं, जिनका पालन करने पर एक समझौता डिक्री एक अवयस्क पर बाध्यकारी होगी-
(1) वादमित्र या वादार्थ संरक्षक न्यायालय की इजाजत (अनुमति/अनुज्ञा) के बिना उस वाद में कोई समझौता नहीं करेगा।
(2) ऐसी इजाजत को कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा।
(3) ऐसी इजाजत के लिए वादमित्र या वादार्थ संरक्षक आवेदन करेगा, जिसके साथ उसका शपथपत्र होगा कि- प्रस्तावित करार या समझौता उसकी राय में अवयस्क के फायदे (लाभ) के लिए है।
(4) यदि उस अवयस्क का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर (वकील) द्वारा किया जाता है, तो उस प्लीडर का इस आशय का प्रमाणपत्र और दिया जावेगा कि प्रस्थापित करार या समझौता उसकी राय में अवयस्क के फायदे (लाभ या हित) के लिए है।
उपरोक्त क्रम संख्या (3) व (4) में वर्णित शपथपत्र और प्रमाणपत्र देना आज्ञापक (अनिवार्य) होगा, क्योंकि विधायिका ने यह संशोधन इसी उद्देश्य से किया है कि अवयस्क के हित की पूर्णरूप से रक्षा की जा सके। इसके लिए एक शर्त और जोड़ दी गई है और न्यायालय को विशाल विवेक दिया गया है अर्थात्
(5) उपरोक्त शपथपत्र और प्रमाणपत्र देने के बाद भी न्यायालय को यह जांच करने की शक्ति है कि क्या ऐसा करार या समझौता अवयस्क के फायदे के लिए है?
(6) उपनियम (2) के अनुसार ऐसी लिखित इजाजत के बिना किया गया कोई भी करार या समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्यकरणीय होगा। अतः अवयस्क उसे शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय में कार्यवाही कर सकेगा।
उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर समझौता डिक्री शून्य नहीं हो जाती, न यह न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करती है, परन्तु ऐसी डिक्री उस अवयस्क की इच्छा पर शून्यकरणीय होगी। परन्तु ये निर्णय पुराने हैं। अब न्यायालय द्वारा दी जाने वाली इजाजत के लिए भी उपरोक्त शर्त संख्या (3) व (4) के अनुसार शपथपत्र और प्रमाणपत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है और न्यायालय को फिर भी जांच करने का अधिकार दे दिया गया है। इस प्रकार कठोर-व्यवस्था के बाद भी उपनियम (2) उस समझौता या करार को अवयस्क की इच्छा पर शून्यकरणीय घोषित करता है।
अवयस्क के प्रतिनिधित्व का स्वरूप अवयस्क का हित सर्वोपरि अवयस्क के प्रतिनिधित्व के बारे में मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-
(1) ऐसे मामले, जहां कार्यवाही के आरंभ से ही अवयस्क का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, और (2) ऐसे मामले, जहां अवयस्क का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया, परन्तु वहां कुछ समय संरक्षक ने ठीक काम किया और बाद में वह कुछ कदम उठाने का लोप कर गया। ऐसी स्थिति में श्रेणी (1) के मामले में कार्यवाही शून्य होगी, पर दूसरे में नहीं। किसी मामले में विवाद के क्षेत्र का पता लगाने के बाद उस विवाद को चलाना या नहीं, इसका निर्णय करने की उस संरक्षक को छूट है। क्योंकि यह अवयस्क के हितों की प्रज्ञापूर्ण व्यवस्था का मामला है, जो संरक्षक की क्षमता के भीतर आता है।
"उस वाद के बारे में" (with reference to the suit) यह शब्दावली वाद में प्रश्नगत किये गये तथा डिक्री में घोषित किए गए अधिकारों और दायित्वों तक सीमित है।
शून्यकरणीय डिक्री को चुनौती देना उपनियम (2) के अनुसार अवयस्क को छोड़कर ऐसी डिक्री सभी के विरुद्ध शून्यकरणीय है। अतः यह केवल अवयस्क की इच्छा (आप्शन) पर होने से कोई अन्य पक्षकार इस डिक्री को प्रश्नगत नहीं कर सकता और अवयस्क इसे या तो वयस्कता-प्राप्ति के बाद प्रश्नगत कर सकेगा या इसके पहले अपने वादमित्र के माध्यम से।
एक विभाजन-वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई और नियम 7 (1) की पालना नहीं की गई। इसे न तो अपील में चुनौती दी गई या न कोई अलग से वाद लाया गया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब उस प्रारंभिक डिक्री को अन्तिम डिक्री के विरुद्ध अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती।
अवयस्क के साथ समझौता आदेश 32, नियम 7 के अधीन आवेदन द्वारा अवयस्क की ओर से समझौता करने की अनुमति लिए बिना और उस समझौते के विधिपूर्ण होने की परीक्षा किए बिना समझौता लेखबद्ध करना अवैध है।
अवयस्क के हित के विरुद्ध समझौता अपास्त किया गया जिस वाद में एक अवयस्क पक्षकार हो, तो न्यायालय उस समझौता डिक्री को अपास्त कर सकता है, जिसमें उस अवयस्क के हितों का ध्यान नहीं रखा गया और मनोनियोग का प्रयोग नहीं किया गया। इस मामले में, समझौता एक तरफा था और उस अवयस्क के किराया कानून में सभी अधिकारों का त्याग तथा किराये की बकाया का भी त्याग कर दिया गया था, जो अवयस्क के हित के विपरीत है।
हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के अवयस्क के प्रतिनिधित्व का प्रश्न-
एक हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा लाए गए वाद में एक अवयस्क भी था। न्यायालय की स्वीकृति के बाद समझौता डिक्री पारित की गई। इस मामले में अवयस्क का कोई अलग हित नहीं था। अतः कुटुम्ब के प्रौढ सदस्यों द्वारा किए गए समझौते को न्यायालय ने अवयस्क के हित में घोषित किया। इसके बाद अवयस्क की ओर से उस समझौता डिक्री को एक वाद में प्रश्नगत किया कि- कुछ उचित सामग्री न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई, जो अवयस्क के हित के बारे में आवश्यक थी। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और उस डिक्री को अवयस्क पर बाध्यकर माना गया।
जब अवयस्क का हित सुरक्षित जहां अवयस्क का हित सुरक्षित रखा गया और कोई कपट या मिली भगत स्थापित नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित समझौता के आवेदन पर समझौता डिक्री पारित करने को टाला नहीं जा सकता।
अवयस्क के वाद का प्रत्याहरण (वापस लेना) विक्रय के करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद को एक प्रत्याहरण-मीमो के आधार पर, जो उस अवयस्क के वाद मित्र बताये जाने वाले व्यक्ति ने फाइल किया था, खारिज कर दिया गया। परन्तु ऐसे प्रत्याहरण के लिए न्यायालय की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद उसके वादमित्र द्वारा कपट के आधार पर उस वाद के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया गया और उस आवेदन के लम्बित रहते वह अवयस्क भी वयस्क हो गया।
अभिनिर्धारित कि- अवयस्क को उस खारिजी के आदेश को न्यायालय की अनुमति नहीं लेने के आधार पर अपास्त कराने का अधिकार है। कपट के लिए अन्य कोई प्रमाण की और आवश्यकता नहीं है, जहां तक अवयस्क प्रार्थी का संबंध है। वयस्कता प्राप्त करने पर उसे अलग से वाद फाइल करने की आवश्यकता नहीं है और वादमित्र द्वारा फाइल किए गए वाद को चालू रखने का उसे अधिकार है।
समझौता निष्पादन में भी संभव यह नियम उन मामलों को भी लागू होता है, जिनमें डिक्री पारित करने के बाद समझौता करना चाहा गया हो। हालांकि नियम वाद के विचाराधीन होने पर ही राजीनामा/समझौता करना अनुध्यात करता है, परन्तु निष्पादन की कार्यवाही उस वाद का निरन्तरीकरण (Continuation of the suit) है। अतः वहां यह नियम लागू होगा 5 और निष्पादन की कार्यवाही में समझौता किया जा सकेगा। परन्तु इस नियम के अधीन समझौता पूरा होने के पहले ही न्यायालय की अनुमति लेने के मत को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है।





 Advertise with us
Advertise with us