सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह : क्या भारत में इसकी पहचान का समय आ गया है?
Yashdeep Chahal
30 July 2020 11:00 AM IST
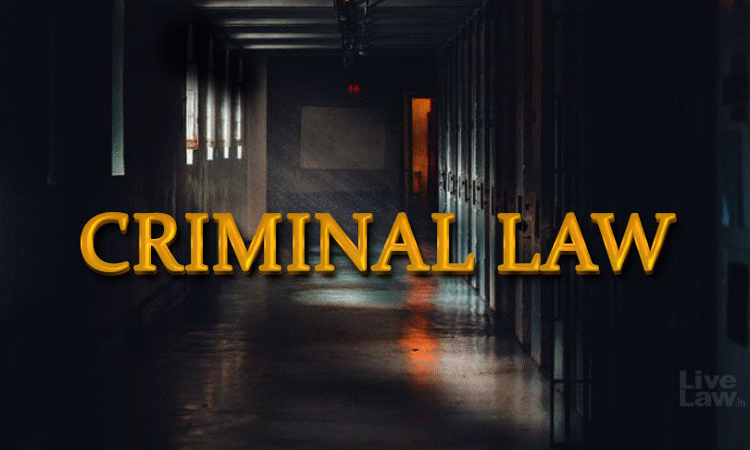
भारत की संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान के ड्राफ़्ट पर चर्चा के दौरान एक शब्द समूह का प्रयोग हुआ - "संवैधानिक नैतिकता" (constitutional morality") का । बाबा साहेब अंबेडकर ने इसका प्रयोग किया और इसे 'ग़ैर-स्वाभाविक भावना' बताया जिसे भारतीय समाज को अपने अंदर विकसित करना है।
भारतीय समाज को बाबा साहेब अंबेडकर ने 'आवश्यक रूप से अलोकतांत्रिक' बताया। इसे समाज का ग़ैर-स्वाभाविक भावना बताते हुए बाबा साहेब ने संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के बीच विवाद की एक रेखा खींची। यह रेखा आज भी मौजूद है। समाज का अलोकतांत्रिक रवैया क़ानूनी मशीनरी में अमूमन दिख जाता है और आपराधिक क़ानून में तो यह अपने बहुत ही ख़राब स्वरूप में हमारे सामने होता है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा समझा जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आपराधिक न्याय व्यवस्था का सर्वाधिक मौलिक तत्व हैं।
व्यावहारिक रूप से यह निष्पक्षता अमूमन सामाजिक वास्तविकताओं का शिकार हो जाता है। यह वास्तविकता, जैसा कि हम देखेंगे, समाज में उस समय मौजूद नैतिकता की स्तर का पैदाइश होती है और यह आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों में परिलिक्षित होती है।
आपराधिक प्रक्रिया सुनवाई और सुनवाई के पूर्व शुरू की जाती है। वैसे अगर इसके व्यापक स्वरूप को देखें, तो यह एक समग्र इकाई लगती है क्योंकि सुनवाई-पूर्व स्तर पर जो अनौचित्य हुआ उसका बाह्य प्रभाव सुनवाई की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। सीधे-सीधे कहें तो सुनवाई को अदालत कक्ष के भीतर अभिमंचित किया जाता है। हालाँकि, अंततः अदालत कक्ष में जो होता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप में अदालत के बाहर होने वाली घटनाओं से नियंत्रित होता है।
गवाहों के बयान, उनकी पेशी, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से निजी पूछताछ, अभियोजन की निष्पक्षता, जाँच के दौरान पुलिस का अनुशासन, साक्ष्य की कोर्ट में सफल पेशी, बार की भूमिका, सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग आदि आपराधिक सुनवाई के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अदालत के कक्ष के बाहर होने वाली सुनवाई-पूर्व घटनाओं से नियंत्रित होते हैं। इस तरह सुनवाई-पूर्व घटनाएँ, जिनमें पूर्वाग्रह पैदा करने की पूरी क्षमता होती है, को हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी सुनवाई की निष्पक्षता पर इनके संभावित असर की जाँच होनी चाहिए। अभी तक हमने इस तरह के की किसी भी जाँच को टालते आए हैं।
सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह
"सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह" एक उधार की अभिव्यक्ति है। इसे रिडो बनाम लूईज़ीऐना से उधार लिया गया है और इस अभिव्यक्ति का प्रयोग अमूमन आपराधिक सुनवाइयों में ज्यूरी की पूर्वाग्रह के लिए होता है। ज्यूरी व्यवस्था में समुदाय के कुछ सदस्य होते हैं जो आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय करते हैं और चूंकि ये सदस्य समुदाय के ही होते हैं, कोई पेशेवर जज नहीं होते, ये कुछ सामाजिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। जब इस तरह की सामाजिक पूर्वाग्रह निर्णय लेने की योग्यता को प्रभावित करती हैं तो यह सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह की स्थिति पैदा करते हैं।
"पूर्वाग्रह" (prejudice) के पहले "सुनवाई-पूर्व" शब्द-समूह का प्रयोग इस बात का संकेत है कि इस तरह की पूर्वाग्रह की पैदाइश उनको आपराधिक सुनवाई का हिस्सा बनाए जाने के पहले उनके सामाजिक और सामुदायिक अनुभवों से हुआ। इंडियन ज्यूरी एक्ट, 1826 के माध्यम से भारत में ज्यूरी व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1973 में संहिता के बनाए जाने तक यह प्रयोग में रहा। बहुप्रसिद्ध नानावटी सुनवाई के दौरान ज्यूरी पूर्वाग्रह के प्रदर्शन को देश ने देखा जिसमें ज्यूरी ने 8-1 से आरोपियों को बरी किए जाने का फ़ैसला दिया। सेशन जज आरबी मेहता ने हाईकोर्ट को इस मामले की समीक्षा का सुझाव देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हमारी पूरी क़ानून व्यवस्था ट्रायल पर है।"
हालाँकि, ज्यूरी व्यवस्था, जैसा कि बाद में पता चला, सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह का एकमात्र कारण नहीं है। यह कई संभावित कारणों में से एक है और यद्यपि हमने ज्यूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, इसके अन्य कारण आज भी क़ायम हैं। आज, भारत का आपराधिक न्याय व्यवस्था सूचनात्मक पूर्वाग्रह के ख़तरे को झेल रहा है। भारत में ऐसा कोई भी क़ानून नहीं है जो आरोपी कि पहचान की रक्षा कर सके। अपराध की सूचना के समय से लेकर मीडिया की रिपोर्टिंग जाँच के समानांतर चलती है। इसके ठीक बाद अदालत के बाहर होने वाला विमर्श शीघ्र ही अदालत में होनेवाली सुनवाई को प्रतिकूलतः प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। चलिए इसकी और आगे पड़ताल करते हैं।
प्रैक्टिस में पूर्वाग्रह
इसको समझने के लिए हमें उन तत्वों को समझने की ज़रूरत है जो एकसाथ मिलकर आपराधिक सुनवाई की संरचना का निर्माण करते हैं। एक निर्णय तक पहुँचने में जज को पेशेवर वकीलों, निष्पक्ष अभियोजकों, बेदाग़ गवाहों और अनुशासित जाँच अधिकारियों की मदद की ज़रूरत होती है। एक न्यायिक अधिकारी के पेशेवर होने का कोई मतलब नहीं है अगर उसे इस प्रक्रिया में कोई मदद नहीं मिलती है। न्याय का लक्ष्य एक सामूहिक कार्य है। आइए मैं इसके बारे में बताता हूं।
एक व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप लगता है क्योंकि उसने एक भाषण दिया है जिसे इंटरनेट पर प्रसारित किया जाता है, उसे तोड़ा-मरोड़ा जाता है और इसके बारे में व्यापक चर्चा होती है, बहुत संभावना है कि उसके ख़िलाफ़ मामले को बंद करने के बजाय चार्ज-शीट दाखिल कर दिया जाए। जिस नृशंस बलात्कार कांड की चर्चा चारों ओर हुई है, इस बात की काफ़ी आशंका है कि उसके गिरफ़्तार आरोपी को हिरासत में हिंसा का सामना करना पड़े और यह सिर्फ पुलिस के ही हाथों नहीं बल्कि जेल में बंद अन्य क़ैदियों से भी।
सामूहिक बलात्कार के "4 संदिग्धों" को फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार देना इसका एक पाठ्य पुस्तकीय उदाहरण है कि समुदाय में ज़रूरत से अधिक विमर्श किस तरह सुनवाई से पहले पूर्वाग्रह पैदा करता है। इन चारों संदिग्धों के फ़ोटो, उनके नाम और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारियाँ सार्वजनिक हो गयी थीं और उनके ख़िलाफ़ यह आजीवन पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए हैं। क्या पुलिस ने उनकी जानकारी प्रकाशित करने से पहले उनकी पहचान ठहराने के लिए इंतजार किया? नहीं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज को संतुष्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा।
फिर, उस मेडिकल ऑफ़िसर की क्या हालत होगी जो खुद अपने बलात्कार की खबर के हर जगह प्रसारित होने से लेकर उस आरोपी के ख़िलाफ़ हुए हिरासत में हिंसा के बाद उसे उस अपराध को लेकर उसके समक्ष पहचान के लिए लाया गया?
चलिए कुछ और बातों पर ग़ौर करें। एक पिछड़े समुदाय में रहने वाला गवाह से सम्मान के लिए होने वाली हत्या (honour killing) को लेकर अदालत में निर्भीक होकर गवाही देने की उम्मीद कम है और वह भी तब जब इस मुद्दे पर समुदाय में काफ़ी बहस हो चुकी है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बार एसोसिएशन्स प्रस्ताव पास कर वकीलों से ऐसे आरोपियों की पैरवी करने से मना करते हैं जो इस तरह के अपराधों में शामिल होते हैं।
इस तरह के बार एसोसिएशन्स स्थानीय भावनाओं से खुद को जोड़कर देखते हैं जो सज़ा के समर्थन में होते हैं। तो क्या उस स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि इस तरह के आरोपी को अदालत में अपने पसंद का वक़ील पैरवी के लिए नहीं मिल पाएगा? इस मामले पर अनुच्छेद 22 में जोर दिया गया है जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है।
ये सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह के उदाहरण नहीं हैं?
क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा सूचना के परिणाम नहीं हैं?
क्या ये सुनवाई की निष्पक्षता के ख़िलाफ़ नहीं है (यह मानते हुए कि सुनवाई की स्थिति आ गई है)?
कारण
ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उससे पता चलेगा कि पूर्वाग्रह एक समान घटना नहीं है। पर इसकी कुछ उचित व्याख्या मौजूद है। इसकी शुरुआत समय से पूर्व ही ज़रूरत से ज़्यादा सूचना के होने से है। जब अपेक्षाकृत जानकारी रहित समाज में किसी जघन्य अपराध को मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज मिलता है और इस क्रम में आरोपी की पहचान को बचाने की कोई कोशिश नहीं होती है तो पूरा समुदाय पीड़ित की पीड़ा को साझा करना शुरू करता है और यह कहना शुरू कर देता है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा से कम उनको कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। फिर निष्पक्षता में अंतिम कील ठोक देता है मूलभूत क़ानूनी जानकारी का नहीं होना और मीडिया और आम नागरिकों में निर्दोष होने का अनुमान । इसका प्रभाव अकल्पनीय है और अभी तक इसकी पड़ताल नहीं की गई है। इस बारे में जज मत्सच की बातें याद आती हैं जिन्होंने अमेरिका बनाम मैक वे मामले में कहा कि "पूरा देश एक एकीकृत समुदाय बन गया है जो उन लोगों के भावनात्मक अभिघात का अनुभव करता है जिन्हें प्रत्यक्षतः पीड़ित बना दिया गया है।"
दंडित करने के इस सामूहिक उत्साह में उन लोगों के निष्पक्ष और मुक्त विचारों की बलि चढ़ जाती है जो विभिन्न स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं – पुलिस, गवाह, डॉक्टर, विशेषज्ञ, वक़ील, अभियोजक आदि। उनको लगता है कि उन्हें समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है और इस तरह वे सुनवाई में एक कमजोर कड़ी साबित होते हैं। स्थानीय भावनाएं संवैधानिक भावनाओं पर भारी पड़ जाती हैं। ज़ाहिर है, इनके कारण लगातार बदल रहे हैं। तथ्य यह है कि कारणों की इन जटिलताओं ने इन अनौचित्यों को क़ानून की गिरफ़्त में आने से रोक देता है। हम इसे "चलता है" के सिद्धांत का हिस्सा मानते हैं।
सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रह सिर्फ़ आरोपियों के ख़िलाफ़ ही काम नहीं करता। पीड़ित को भी आए-दिन इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है।
हम ज़रा बॉलीवुड की हर एक फ़िल्म में दिखाई जाने वाली उस कहानी पर ग़ौर करें जिसमें गाँव के कुछ धनी लोग गाँव की एक ग़रीब लड़की का सामूहिक बलात्कार करते हैं। इस घटना के बाद गवाहों को अगवा कर लिया जाता है, सबूतों को दबा दिया जाता है और क़ानूनी मदद देने से इनकार कर दिया जाता है।
स्थानीय मीडिया इसे आत्महत्या करार देता है और पुलिस और गवाहों के लिए इतना ज़्यादा भावनात्मक उबाल पैदा कर देता है कि वे 'सही' दिशा लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है – क्या ट्रायल कोर्ट अन्य पीड़ितों की तरह ही इस तरह के पीड़ितों के लिए भी उन्हीं शर्तों पर खुला है? इससे भी बड़ा प्रश्न है – क्या हमारे ट्रायल कोर्ट इस तरह के पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए सभी ज़रूरी बातों से लैस हैं?
शेपर्ड बनाम मैक्स्वेल (1966) मामले में कहा गया "वर्तमान संवाद की व्यापकता और न्याय करनेवालों के मन से दुराग्रहों को समाप्त करने में आनेवाली कठिनाई को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट को हमेशा ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी के ख़िलाफ़ संतुलन नहीं बने।"
मैं यहाँ 'न्याय करने वालों' (juror) की जगह सुनवाई के अन्य उपांगों को रखना चाहूँगा जिसमें शामिल हैं पुलिस, गवाह मीडिया आदि – और यह कहूँगा कि ट्रायल कोर्ट के लिए यह ज़रूरी है कि वह सुनवाई शुरू होने से पहले की स्थितियों को नियंत्रित करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि हमारी व्यवस्था में शक्ति का संतुलन व्यापक रूप से आरोपी के ख़िलाफ़ है।
क़ानून क्या कहता है?
ऊपर में जिन बातों का ज़िक्र किया गया है उसका उपचार भारत के उच्चतर अदालतों में मौजूद है – या तो संविधान के तहत रिट के द्वारा या आपराधिक प्रक्रिया के तहत अपील के माध्यम से। रिट की जहां तक बात है, यह अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं है और आपराधिक प्रक्रिया के तहत अपील बाद के स्तर पर ऐसे समय आता है कि सुनवाई से पूर्व जो हानि हुई उसकी पुष्टि असंभव हो जाती है। भारत में आपराधिक प्रक्रिया और सबूत के क़ानून में इस तरह की पूर्वाग्रहओं को रोकने का उपाय नहीं है। उनमें इसके उपचार का प्रावधान है और अपीली अदालतों में किसी उपचार का प्रावधान करने से पूर्व "न्याय की विफलता" को साबित करने की पूरी ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई है।
जब हम 'पूर्वाग्रह' के प्रति न्यायविधान के नज़रिए को समझते हैं तब पता चलता है कि इसमें कितनी ज़्यादा चुनौतियां हैं।
उदाहरण के लिए मोहम्मद हुसैन बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी सरकार) मामले में कोर्ट ने कहा,
"… 'पूर्वाग्रह' की आम व्याख्या नहीं हो सकती और इसे आपराधिक न्यायविधान में लागू नहीं किया जा सकता। पूर्वाग्रह की दलील जाँच या सुनवाई के बारे में ही हो सकती है और उन मामलों के बारे में नहीं जो उनकी परिधि के बाहर है।"
अब समय आ गया है जब हम यह मानें कि जाँच और सुनवाई के परंपरागत स्तर के बाहर भी पूर्वाग्रह की संभावना है। "जाँच" के सीमित अर्थ को हम जैसे ही स्वीकार करते हैं, तो इसका असर यह होता है कि ऐसी असंख्य ऐसी परिस्थितियाँ जो मामले में पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, उन्हें इसकी परिधि से बाहर कर देती हैं। इसलिए अब क़ानून इन परिस्थितियों को अपनी परिधि में लाए।
समय का तक़ाज़ा है कि निचली अदालतों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वे सुनवाई-पूर्व पूर्वाग्रहों की स्वतंत्र रूप से जाँच कर सकें भले ही उसका कारण कुछ भी हो – और प्रक्रियागत अनौचित्यों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें । सुनवाई के पुख़्ता आधार के लिए यह ज़रूरी है कि निचली अदालत प्रभावी तरीक़े से कोर्ट के बाहर पैदा होने वाले इन पूर्वाग्रहों का मुक़ाबला कर सके। इन प्रश्नों को अगर अपीली मंचों के लिए छोड़ दिया जाए तो इससे इसकी स्वाभाविकता, निरंतरता और इससे भी अधिक आपराधिक न्याय की व्यवस्था में विश्वास की कमी पैदा होगी।
चूंकि हर पूर्वाग्रह का अपनी भूमिका का निर्वाह करने और सुनवाई को नुक़सान पहुँचाने के बाद उसका पता नहीं लागाया जा सकता, उसकी पहचान नहीं की जा सकती और उसको सूचिबद्ध नहीं किया जा सकता। अपीली स्तर पर उसके प्रभाव को न्याय की विफलता के रूप में हमेशा साबित नहीं किया जा सकता है। इस बात का समय भी आ गया है जब आईपीसी की धारा 228A जैसे प्रावधान बनाए जाएँ ताकि आरोपी की पहचान की सुरक्षा की जा सके।
आरोपी को "सूचनात्मक निजता" और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है भले ही इसके लिए प्रेस पर कुछ प्रतिबंध क्यों न लगाना पड़े। मेरी राय में संतुलन का झुकाव आरोपी के पक्ष में होता है। इससे पहले कि क़ानून खुद ट्रायल का विषय बन जाए, जिन कारणों से पूर्वाग्रह पैदा होती है उनको कानून के हवाले किया जाना ज़रूरी है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)





 Advertise with us
Advertise with us